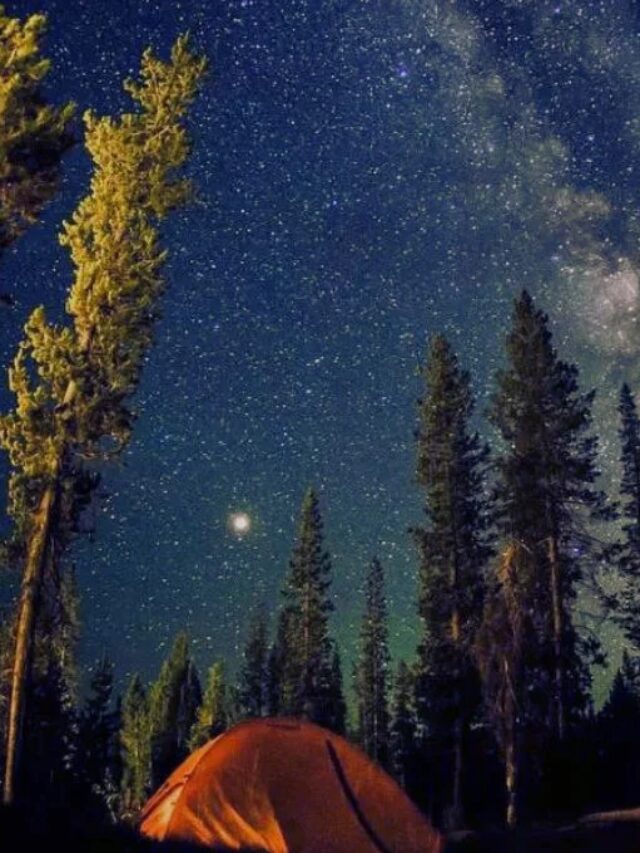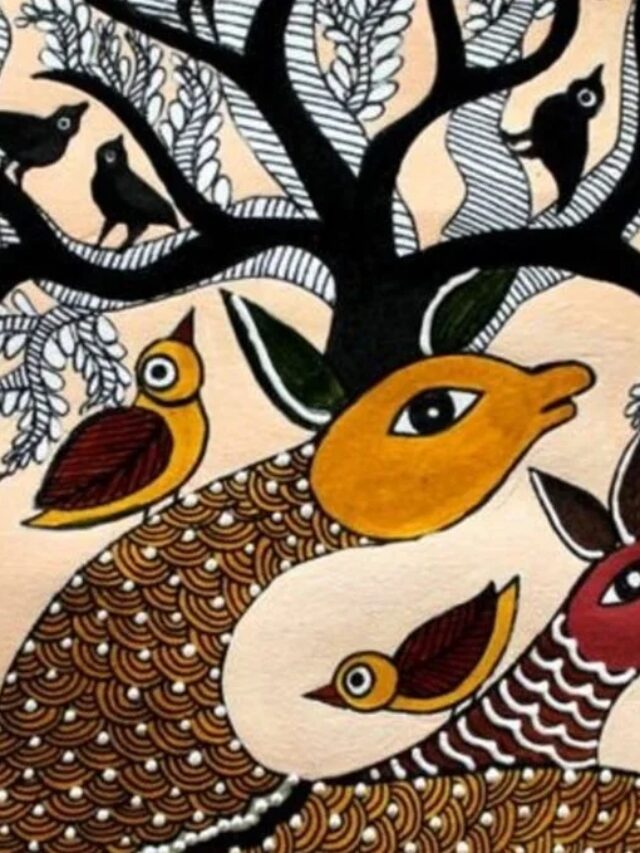रीवा सूद और उनके पति राजीव, कई सालों से दिल्ली में भाग-दौड़ वाली जिंदगी जी रहे थे। अपनी लाइफस्टाइल के ओर उनका ध्यान तब गया, जब 2012 में उन्हें पता चला कि राजीव कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। इस खबर से दोनों को ही बड़ा झटका लगा और उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला किया।
दोनों ने अपने लाइफस्टाइल सहित खान-पान पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जो सब्जियां वे खाते हैं उनमें काफी मात्रा में जहरीले तत्व मौजूद थे, जो दुनिया भर में कई तरह की बीमारियों का कारण हैं। रीवा और राजीव को लगा कि शायद कैंसर जैसी बीमारी में इसका भी योगदान हो सकता है।
बस यहीं से उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया। उन्होंने न केवल हिमाचल के ऊना जिले में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की, बल्कि ‘Him2Hum’ नाम से एक कंपनी भी शुरू की, जिससे वहां रहनेवाली सैकड़ों महिलाएं सशक्त बन रही हैं।
रीवा, पिछले 30 सालों से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं। द बेटर इंडिया के साथ बात करते हुए वह कहती हैं, “राजीव का कैंसर होना हमारी माइंडसेट में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया।”
ऑर्गेनिक खेती में सफलता के लिए लिया बड़ा रिस्क

छह साल पहले, रीवा ने 30 एकड़ बंजर ज़मीन के सामने खड़े होकर खुद से यह वादा किया था कि एक दिन इस ज़मीन को न केवल हरा-भरा बनाएंगी, बल्कि गाँव की महिलाओं के आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाएंगी।
धीरे-धीरे रीवा का खुद से किया वादा वास्तविकता में बदलने लगा। कुछ ही सालों में उस 30 एकड़ ज़मीन पर अच्छी मात्रा में शतावरी, सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, स्टीविया, हरसिंगार, एलोवेरा, वीटिव ग्रास, लेमन ग्रास आदि उगने लगे। जो जगह कभी बंजर और खाली ज़मीन हुआ करती थी, वहां 2019 तक 17 किस्मों की फसलें उगाई जाने लगीं।
रीवा ने आगे थोड़ा रिस्क लिया और दो ऐसी फसलें उगाने का सोचा जो मेनस्ट्रीम में शामिल नहीं हैं। वे फसलें थीं- काला गेहूं और ड्रैगन फ्रूट। रीवा कहती हैं कि उन्होंने इन फसलों की क्षमता देखी और उन पर विश्वास किया। सुपरफूड माने जाने वाले इस फसल के बारे में वह कहती हैं, “हम गेहूं के विकल्प के रूप में काले गेहूं को पेश करना चाहते थे।”
इसके अलावा, ड्रैगन फ्रूट के लचीलेपन के कारण वह इसकी ओर आकर्षित हुईं। रीवा कहती हैं कि उन्हें पता था कि वह एक फसल उगाने का रिस्क ले रही हैं। वह कहती हैं, “मुझे कुछ ऐसा चुनना था, जो गर्म क्लाइमेट और कभी-कभी सूखे जैसी स्थितियों में भी जीवित रह सकें।”
यहां के किसान भी यह फल उगाने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके पीछे उनके कारण अगल हैं।
केमिकल के बजाय, स्थानीय रूप से उपलब्ध चीज़ों का करती हैं इस्तेमाल

गांव के ही एक किसान, शमी का कहना है कि पहले, बंदर उनकी फसलों को खा जाते थे, लेकिन फलों की कांटेदार बनावट उन्हें दूर रखती है। वह आगे कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती के बिज़नेस का हिस्सा होना उनके लिए एक नया अनुभव रहा है।
शमी ने बताया, “इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। यह एक नया फल है और हम इसे पहली बार देख रहे हैं। शुरुआत में इसे लेकर हमें थोड़ा संदेह था। लेकिन हमने देखा कि एक-एक फल 80 रुपये में बेचा जा रहा था और फिर हमने महसूस किया कि हमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है।”
इन खेतों में उगने वाले फसलों की मात्रा का एक मोटा अंदाजा रीवा को मिलने वाले ऑर्डर से लगाया जा सकता है। पीक सीज़न के दौरान, उन्हें सर्पगंधा के करीब 900 ऑर्डर मिलते हैं।
ऑर्गेनिक खेतों पर केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। केमिकल की बजाय, ज़मीन को पोषण देने और उपजाऊ बनाने के लिए गौ मूत्र, गाय का गोबर, पंचगव्य, नीम स्प्रे और लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी सामग्रियां स्थानीय रूप से उपलब्ध होती हैं, लेकिन अक्सर इन्हें ‘बेकार’ माना जाता है।
रीवा बताती हैं कि इस ज़मीन के टुकड़े को बदलने में उन्हे छह साल का वक्त लगा। लेकिन असल में यह काम बहुत अलग था। उन्होंने बताया, “मेरे मन में किसानों को लेकर एक अलग छवि थी, जो सिनेमा आदि देखकर बनी थी।”
ऑर्गेनिक खेती के बारे में किसानों को समझाना था मुश्किल काम

रीवा हमेशा से दिल्ली में रहीं और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह काम इतना ज्यादा कठिन होगा। कई बार उन्होंने बाहर 40 डिग्री तापमान में भी काम किया, लेकिन इन मुश्किलों से उन्होनें हिम्मत नहीं हारी।
समय के साथ, धीरे-धीरे ऑर्गेनिक खेतों पर अच्छी फसलें उगने लगीं और फिर 10 और किसान रीवा के साथ आए। आज, वे 10 किसान पूरे समय खेत में रहते हैं और काम करते हैं। इससे रीवा को दिल्ली में अपने घर और हिमाचल में खेत, दोनों देखने में काफी मदद मिलती है।
शमी कहते हैं कि उन्हें मुनाफे के अलावा भी कई तरह का फायदा हुआ है। वह कहते हैं, “हम कई तरह के पौधों को उगाना और खेती करना सीखते हैं। यह हम बिना किसी के समर्थन के कभी नहीं कर पाते।”
रीवा कहती हैं कि केमिकल-मुक्त खेती के लिए किसानों को साथ लाना एक कठिन काम था। ज्यादातर किसान, खेत में फसल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का काफी संदेह था कि ऑर्गेनिक खेती से अच्छी फसल मिल पाएगी या नहीं। लेकिन एक बार जब ऑर्गेनिक खेती का परिणाम दिखना शुरू हो गया, तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
Him2Hum का क्या मकसद है?

एक बार जब ऑर्गेनिक खेती ने गति पकड़ना शुरू कर दिया, तब रीवा इस काम को कमर्शिअलाइज़ करना चाहती थीं। इसके अलावा, वह महिलाओं को बिज़नेस के मुख्य काम-काज में शामिल भी करना चाहती थीं। इस तरह, 2016 में उन्होंने एक वुमन फार्मर प्रोड्युसर (महिला किसान निर्माता) कंपनी Him2Hum की शुरूआत की।
इस बिज़नेस का एक साधारण लक्ष्य था – गाँव की महिलाओं को खेती करने, फसल उगाने, उत्पादन करने, खेती की प्रक्रिया,कटाई के बारे में ट्रेन करने और कृषि उपज व मेडिसिनल हर्ब्स के कारोबार की समझ देना। इसके अलावा, यहां उगाई जाने वाली उपज के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मार्केटिंग और डिस्ट्रिब्युशन का भी ख्याल रखा जा रहा है।
यह वह संदेश है, जिसके ज़रिए रीवा ऊना की महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती थीं। रीवा बताती है, “जब मैं पहली बार यहां आई थी, तो मैंने देखा कि भले ही महिलाएं मक्खन बनाती हैं और खेतों में जाती हैं, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट या काम को औपचारिक रूप से करने के लिए कहा जाता है, तो काफी संकोच करती हैं।”
रीवा कहती हैं कि वह इस संकोच को हटाकर समानता लाना चाहती थीं और सुनिश्चित करना चाहती थीं कि हर महिला के पास अपना पैन कार्ड और हस्ताक्षर करने का अधिकार हो।
सैकड़ों महिलाओं को मिली आर्थिक स्वतंत्रता

वर्तमान में, 230 महिलाएं HIM2HUM का हिस्सा हैं। यहां कि एक सदस्य, सुलोचना कहती हैं कि इस बिज़नेस का हिस्सा बनने के बाद, वह पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र महसूस करती हैं। वह कहती हैं, “मैं खेतों में काम करती हूं और विभिन्न फसलों की जैविक खेती में मदद करती हूं। प्याज, लहसुन और अन्य फल भी हैं, जिन्हें हमने इस क्षेत्र में पहले नहीं देखा था। लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि मैं कह सकती हूं कि मैं अब कामकाजी हूं और मेरे पास भी स्किल है।”
आज ऊना, ऑर्गेनिक खेती के ज़रिए खेती करने के पुराने तरीकों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तकनीकों में नए बदलाव देख रहा है, जिससे स्थानीय आबादी को फायदा पहुंच रहा है। इसके साथ ही, यहां की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, उन्हें समर्थन दिया जा रहा है और साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी सिखाया जा रहा है। इसके अलावा, महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।
रीवा ने तहसील पर भी जोर दिया है, ताकि महिलाओं का किसान बुक में नाम होना अनिवार्य बनाया जा सके। सुलोचना कहती हैं कि वह भी इन महिलाओं में से हैं, जिन्हें इन सारी चीजों का फायदा हुआ है और इस तरह, खेती पर उनका हिस्सा बराबर का होगा।
ऑर्गेनिक खेती के ज़रिए लोगों की बदल दी सोच

ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल के साथ, रीवा ने काम न आने वाली और बेकार समझी जाने वाली चीजों के प्रति लोगों के रवैये में बदलाव लाने की भी कोशिश की है। उदाहरण के लिए, जब वह पहली बार ऊना आईं, तो देखा कि बूढ़ी गायों या नर बछड़ों से किसी को कोई फायदा नहीं था। वे एक तरह से जिम्मेदारी बन जाते थे और फिर अंत में उन्हें बूचड़खाने ले जाया जाता था।
ये सब देखना उनके लिए काफी भयावह था। जांच-पड़ताल करने पर, ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास जानवरों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। वह कहती हैं, “मैंने कुछ दिन इस पर विचार किया और फिर खेत पर ही एक शेड बनाया। मैंने ग्रामीणों से अपनी गायों को लाने के लिए कहा। हालांकि ये मेरे भी किसी काम के नहीं थे।”
फिर रीवा ने वर्मिकम्पोस्ट गड्ढे के लिए जानवरों से गाय के गोबर का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह कहती हैं, “यह एक उदाहरण बन गया कि अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए, तो बेकार समझी जाने वाली चीजें भी उपयोगी हो सकती हैं।”
इसके साथ ही, रीवा ने ग्रामीणों को ज़मीन पर बनाए गए गड्ढे में कचरे के छिल्के, लस्सी आदि को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे जीवाम्रृत बनता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है।
कितना सफल रहा यह आईडिया?

अब गांववाले, समय के साथ और भी कई चीज़ें सीख रहे हैं। HIM2HUM को नेशनल लेवल बैंक फॉर फार्मर्स, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और नाबार्ड से फंड मिला है। आज इनके पास कई क्लाइंट हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों खिलाड़ी शामिल हैं।
रीवा कहती हैं, “हमारे उत्पादों को पंचायत बेहर जसवा, एएमबी, ऊना एच पी सी/ओ डीआरडीए मग्रेगा जैसी सरकारी अधिकारियों और दवा कंपनियां जैसे स्वाति स्पेनटोज प्राइवेट लिमिटेड, केटाव्स आयुष स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और बायोस्फीयर क्लिनिकल द्वारा खरीदी जाती हैं।”
वह कहती हैं, “यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा लक्ष्य और ऊपर जाने का है। हम अपनी महिला किसानों को ग्लोबल बिजनेस चलाने के पहलुओं के बारे में सिखाना चाहते हैं।”
वह कहती हैं, जिस दिन महिलाएं बड़े मंडी में एक खरीदार के सामने खड़ी हो सकेंगी और बिना किसी के समर्थन के उनसे बात कर सकेंगी, वो उनके लिए बेहतर होगा।
मूल लेखः कृष्टल डिसुजा
संपादनः अर्चना दुबे
यह भी पढ़ेंः 70 की उम्र में दिन के 12 घंटे करते हैं काम, सालभर में बेच लेते हैं 7000 बैग्स ऑर्गेनिक खाद
We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: