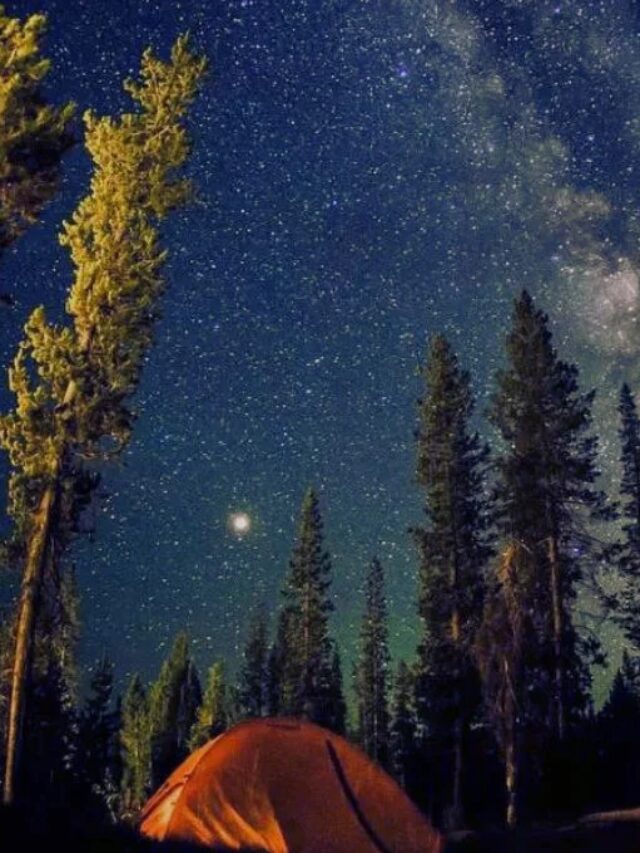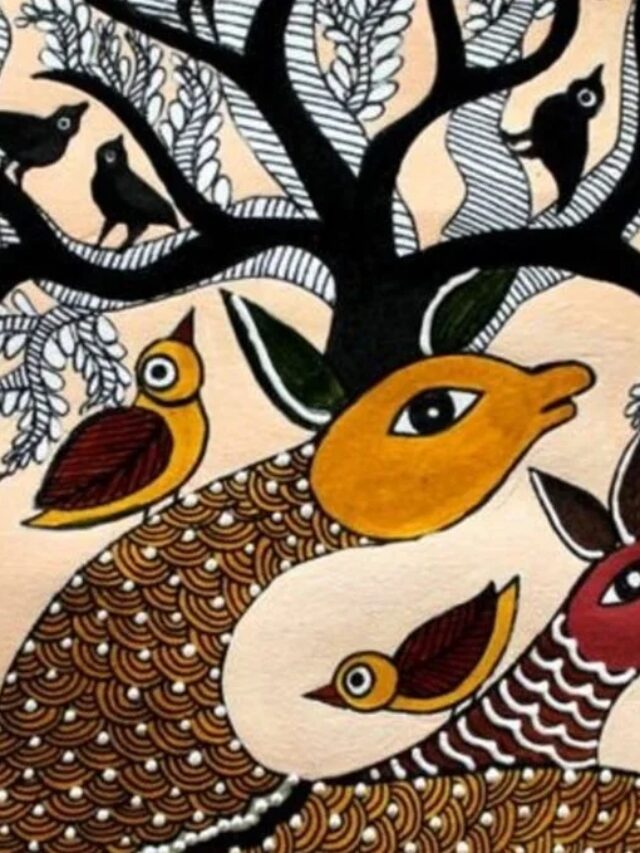उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित टिकरी गाँव के रहने वाले 63 वर्षीय किसान, राम अभिलाष पटेल पिछले दो दशक से जैविक खेती कर रहे हैं। मात्र ढाई एकड़ ज़मीन पर वह गेहूं, चावल और मौसमी सब्जियों की फसल के साथ-साथ मछली पालन भी कर लेते हैं। साथ ही, वह जैविक खाद भी बनाते हैं। इस तरह से अलग-अलग प्रकार की खेती और अतिरिक्त आय के साधनों से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि 12वीं पास यह किसान अपने फसल को मंडी की बजाय सीधा ग्राहकों को पहुंचाता है।
पटेल ने द बेटर इंडिया को बताया, “अगर मैं सब्ज़ियां मंडी में भेजूं तो वहां मुझे मेरी लागत और मेहनत के हिसाब से दाम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने शहरों में अपना नेटवर्क बनाया हुआ है और मैं सीधा ग्राहकों को अपने उत्पाद पहुंचाता हूं। मैंने अपने साथ में अन्य किसानों को भी जोड़ा हुआ है ताकि हम सभी मिलकर जैविक उगाएं और लोगों तक जैविक पहुंचाएं। इससे देश के नागरिकों को स्वस्थ आहार मिल रहा है और हम किसानों को मेहनत का सही दाम।”
हालांकि, राम अभिलाष पटेल की खेती के बारे में और बहुत-सी उपलब्धियां हैं जो उन्हें सिर्फ जैविक किसान नहीं बल्कि किसान वैज्ञानिक बनाती हैं। पटेल ने लगभग 25 बरस पहले चावल की फसल लगाने के लिए एक नई तकनीक ईजाद की थी। इसमें लागत और समय दोनों कम लगता है। इस तकनीक से आप सीधा अपने खेत में धान लगा सकते हैं, आपको पहले नर्सरी में पौध बनाने की और फिर उसे खेतों में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धान लगाने की इस विधि को उन्होंने ‘गोली विधि’ नाम दिया, जिसे अंग्रेजी में ‘क्ले पैलेट’ मेथड कहते हैं।
कहां से मिला आईडिया:

पटेल बताते हैं कि उनके यहां धान से चूड़ा बनाने वाली मशीन चल रही थी। वहीं पास में गाँव के कुछ बच्चे खेल रहे थे और वह मिट्टी की गोलियां बना रहे थे। खेल-खेल में उन्होंने इस मिट्टी में पास में पड़े चावलों के दाने भी मिला लिए। पटेल कहते हैं, “मैं भी उन्हें काम करते हुए देख रहा था। उनके जाने के बाद किसी महिला ने इन मिट्टी की बनी गोलियों को पास के मेरे खेत में डाल दिया। उस समय मेरे मन में कुछ खास नहीं आया लेकिन फिर एक-डेढ़ महीने बीता और तब बारिश हो गई थी तो मैंने अपने खेत में जुताई कर रहा था, तब बैल और हल से यह काम होता था।”
पटेल को जुताई करते समय, खेत के एक कोने में धान के पेड़ दिखाई दिए जो अच्छे से पनप रहे थे। उन्हें पहले तो कुछ अजीब लगा पर फिर उन्हें बच्चों की बनाई मिट्टी की गोलियां याद आईं। उन्होंने उन कुछ पौधों को निकाला तो उनकी जड़ों की मिट्टी भी अलग थी। बस उसी पल उन्हें लगा कि अगर इस विधि से पूरे खेत में धान लगाया जाए तो शायद अलग से पौध लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पटेल, इस विधि को लेकर इलाहबाद के कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे और वहां वैज्ञानिकों को इस बारे में बताया।
वैज्ञानिकों ने उनकी बात सुनी और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह अपने खेत के छोटे-से हिस्से में यह प्रयोग करके देखें। पटेल बताते हैं कि केवीके की मदद से उन्होंने अगले मौसम में 5 बिस्वा ज़मीन के लिए यह गोलियां (क्ले पैलेट) तैयार किए। उन्होंने अप्रैल और मई के महीने में गोलियां बनाकर सूखा लीं। गोलियां बनाने के लिए उन्होंने तालाब की काली मिट्टी का इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें जीवांश अधिक होता है तो यह काफी उपजाऊ होती है।
उन्होंने कहा,”तालाब की मिट्टी लेते समय भी ध्यान रहे कि जिस तरफ की हवा है उस तरफ से मिट्टी लें। इससे खरपतवार के बीज मिट्टी में नहीं बैठते क्योंकि वह हवा से सतह पर ही बहती रहती है। मिट्टी निकालने के बाद अगर यह बहुत पतली है तो इसमें राख मिलाएं न कि बाहर की मिट्टी। अब इसे आटे की तरह गुंथे और इसमें धान के बीज भी मिला लें। जब यह अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप इसकी गोलियां बनाएं। कुछ गोलियां बनाने के बाद देखें कि हर एक गोली में कितने बीज आ रहे हैं। यदि किसी गोली में सिर्फ 1-2 बीज ही हैं तो आप और बीज मिट्टी में मिलाएं।”

गोलियां बनाने के बाद इन्हें धूप में सुखाएं और फिर जून के आखिरी सप्ताह व जुलाई के पहले सप्ताह में इन्हें अपने खेत में लगाएं। समान दूरी पर आप लाइन से खेत में यह गोलियां लगा दें। इसके बाद, जैसे ही पहली बारिश हुई तो पटेल के खेत में पौधे अंकुरित होना शुरू हो गए। कुछ समय पश्चात, उन्होंने सिर्फ एक बार खेत में निराई की। वह कहते हैं कि उन्हें खेत में बहुत पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि धान की जड़ को सिर्फ नमी चाहिए होती है और हमने पहले ही तालाब की मिट्टी से गोलियां बनायीं थीं। जिसमें काफी मात्रा में नमी होती है।
“इसमें लागत भी कम आई क्योंकि नर्सरी तैयार करने के लिए किसी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ी और समय भी बचा। बाद में जब हमने फसल काटी तो हमारा उत्पादन पहली फसल से लगभग एक क्विंटल ज्यादा था। एक-दो बार जब इसी विधि से धान की अच्छी उपज लेने में सफल रहा तो दूसरे किसानों ने भी मुझे जानना शुरू किया,” उन्होंने कहा।
साल 2005 में पटेल की इस अनोखी तकनीक के बारे में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को पता चला। उन्होंने पटेल से न सिर्फ इस तकनीक को समझा बल्कि उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया। पटेल कहते हैं कि किसानों से उनका जितना नेटवर्क जुड़ा और आज वह जहां भी हैं, इसका श्रेय NIF को ही जाता है। NIF ने उन्हें मौका दिया जिससे वह दुनिया भर के अन्वेषक किसानों से मिल पाए और तब से उनकी खेती ने एक अलग राह ले ली।
खेती के साथ मछली पालन भी

पटेल ने इसके बाद अपने धान के खेत में ही मछली पालन शुरू किया। खेत के एक किनारे पर उन्होंने 3 फ़ीट गहरा गड्ढा खोदा, जिसे बाकी तीन तरफ से मेढ़ों से बाँधा गया है। लेकिन खेत वाली तरफ से यह खुला हुआ है। इसमें उन्होंने पानी भर दिया और मछलियां डाल दीं। धान के खेत में थोड़ा-बहुत पानी भरकर रखा जाता है। “दिन में जब गर्मी होती है तो मछलियां गड्ढे में रहती हैं और रात को यह खेत में तैरती हैं। एक बात और मैंने नोटिस की कि पानी रहने से धान के पेड़ों की जड़ों पर अक्सर काई लगने लगती है। मछलियों के लिए यह काई और अन्य छोटे-मोटे जीवाणु उनका चारा होते हैं। इस तरह से आप एक ही खेत में दो फसल ले सकते हैं,” पटेल ने बताया।
पटेल अपने खेत में गेहूं, धान और मछली पालन के साथ मौसमी सब्ज़ियां भी लगाते हैं। उन्होंने अपने खेतों पर ही जैविक खाद बनाने की यूनिट भी लगाई हुई है। इससे उनके खेत को खाद मिलती है और साथ ही, दूसरे किसान भी उनसे खाद खरीदते हैं। सब्जियों को मंडी में बेचने की बजाय, वह सीधा ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। वह कहते हैं कि उन्हें खाद से महीने का 5-6 हज़ार रुपये की कमाई होती है और सब्जियों से हर मौसम में वह लगभग डेढ़ लाख रुपये तक की बचत कर रहे हैं।
खोजा सदाबहार चारा
राम अभिलाष पटेल की एक उपलब्धि यह भी है कि उन्होंने पशुओं के लिए एक हरे चारे की खोज की है। वह कहते हैं कि अपने गाँव से 65 किमी दूर वह एक रिश्तेदार के यहां गये थे। यह बारिश का मौसम था और खूब बारिश हुई तो पास के जंगलों से कुछ पेड़-पौधे बहकर उस गाँव के खेतों के पास पहुंच गये। सुबह पटेल अपने रिश्तेदार के साथ टहलने गए तो उन्होंने देखा कि चारा चरने आए पशु खेतों के बाहर पड़े कुछ पेड़ों को खा रहे हैं। उन्हें लगा कि उन्हें इस पौधे के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए।
पटेल कहते हैं, “मैं वहां से कुछ पौधे ले आया और अपने यहां लगा दिए। जब यह पौधे बड़े हुए तो इन्हें मैंने पशुओं को खिलाया और कुछ जानकारों से इस पर चर्चा की। यह कोई जंगली पौधा था जिसे पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि इस पौधे में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी है। मैंने इसे नित्या घास नाम दे दिया। आज मेरे साथ और भी बहुत से किसान भाई इसे अपने खेतों की मेढ़ों पर उगा रहे हैं।”
सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने साथ अपने इलाके के अन्य किसानों को भी जोड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ समय पहले एक किसान उत्पादक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया है। उनका उद्देश्य है कि वह अपनी फसलों की खुद प्रोसेसिंग करें, जिससे उनके इलाके के किसानों को फायदा हो।
राम अभिलाष पटेल की ही तरह, पंजाब के किसान प्रभात सिंह ने बागवानी में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके पहचान बनाई है।
क्रियात्मक तरीके से लगाए लीची के पेड़:
पठानकोट के चक माधो गाँव में रहने वाले 74 वर्षीय प्रभात सिंह को बागवानी करते हुए 20 साल से भी अधिक हो गए हैं। वह बताते हैं कि वह फलों की उपज लेते हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा उत्पादन लीची का होता है। उन्होंने लीची की फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोग किए। उनके ये क्रियात्मक प्रयोग सफल रहे और आज उनकी गिनती इलाके के अन्वेषक किसानों में होती है।
प्रभात सिंह बताते हैं कि वह काफी समय से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, पंजाब से जुड़े हुए हैं। उनके सहयोग से उन्होंने सबसे पहले अपने बाग में वर्मीकंपोस्ट यूनिट लगाई। इससे उन्हें जो भी उर्वरक खरीदने पड़ते थे, उनकी लागत खत्म हो गयी। साथ ही, इस उत्तम गुणवत्ता की जैविक खाद से उनके फलों की गुणवत्ता भी बढ़ी है।
इसके अलावा, उन्होंने प्लांटेशन के तरीकों में बदलाव किए। “लीची के पेड़ों को धूप अच्छे से मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम पेड़ लगाते हैं और सभी पेड़ों का आकर और लम्बी समान होती है। इससे जो आगे की कतार में पेड़ होते हैं उन्हें तो धूप मिल जाती है लेकिन पीछे के पेड़ों को अच्छे से धूप नहीं मिलती। इस वजह से उन पेड़ों के फल इतने अच्छे नहीं मिल पाते थे, जितने कि आगे के पेड़ों के मिलते थे। इस समस्या के हल के लिए में एक प्रयोग किया,” उन्होंने आगे कहा।

प्रभात ने लीची की दो अलग-अलग किस्में लीं- एक देहरादून और दूसरी कलकत्ती। देहरादून किस्म के पेड़ लम्बे होते हैं और कलकत्ती के छोटे। छोटे पेड़ों को आगे की तरफ लगाया गया और दूसरी पीछे की कतार में लम्बी किस्म के पेड़ों को। इससे समान रूप से सभी पेड़ों को धूप मिलती है। प्रभात के इस तरीके से उन्हें काफी फायदा हुआ। उनके लीची के फलों की गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादन भी बढ़ा। इसी तरह उन्होंने लीची के साथ गन्ने और जामुन के पेड़ों की इंटरक्रॉपिंग भी की है। गन्ने और जामुन के पेड़ उनके लीची के पेड़ों को सर्दियों में ठंडी-सर्द हवाओं से सुरक्षित करते हैं तो गर्मियों में लू से। इससे लीची के फल खराब नहीं होते।
इंटरक्रॉपिंग के साथ-साथ प्रभात सिंह ने अपने फलों की पैकेजिंग की तकनीक भी खुद इजाद की। उन्होंने लुधियाना स्थित पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से चर्चा की और फलों की पैकेजिंग के लिए लकड़ी के डिब्बों की बजाय गत्ते के डिब्बे इस्तेमाल करने की सलाह दी। वहां से सहयोग मिलने के बाद, प्रभात सिंह ने 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो की क्षमता वाले कार्टन बनवाए। उनका कहना है कि इससे मार्केटिंग में आसानी रहती है। अगर किसी को कम फल खरीदने हैं तो उनके पास भी विकल्प होता है कि वह सीधा हमसे खरीद लें।

इस तकनीक से प्रभात सिंह का उत्पादन और प्रॉफिट दोनों बढ़ा। लीची से होने वाली बचत में 50 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ तो गन्ने और जामुन के पेड़ों से अतिरिक्त आय आई। इसके साथ-साथ वह सरसों और कुछ दालें भी उगाते हैं क्योंकि इनकी जड़ों से मिट्टी को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। ऐसा करते रहने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। प्रभात की तकनीकों को जब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सराहा गया तो उनके आस -पास के गांवों में बागवानी करने वाले किसान भी उनसे जुड़े। फ़िलहाल इलाके की लगभग 110 एकड़ ज़मीन पर उनके तरीकों से बागवानी हो रही है।
प्रभात सिंह कहते हैं कि उनके फार्म को लीची उत्पादन के लिए बेस्ट फार्म के ख़िताब से नवाज़ा जा चूका है। इसके अलावा उन्हें कृषि में मुख्यमंत्री अवॉर्ड भी सम्मानित किया गया है।
प्रभात सिंह बताते हैं, “फ़िलहाल, मेरी कोशिश है कि हम लीची की शेल्फ लाइफ बढ़ाएं। इससे बहुत से किसानों को फायदा होगा। मैंने इस बारे में बहुत से कृषि वैज्ञानिकों से बात भी की है और एक-दो प्रयोग भी किए हैं लेकिन यह अभी व्यापक स्तर पर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में लीची के स्टोरेज के लिए भी कोई तकनीक इजाद कर पाएं।”
यह भी पढ़ें: मिर्च की प्रोसेसिंग ने बदली किसानों की ज़िंदगी, लॉकडाउन में भी नहीं रुका काम!
बेशक, राम अभिलाष शर्मा और प्रभात सिंह जैसे किसान पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे।
राम अभिलाष पटेल से संपर्क करने के लिए उन्हें 08127199855 पर कॉल करें और प्रभात सिंह से आज 9815227299 पर संपर्क कर सकते हैं!
यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें, या Facebook और Twitter पर संपर्क करें। आप हमें किसी भी प्रेरणात्मक ख़बर का वीडियो 7337854222 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: