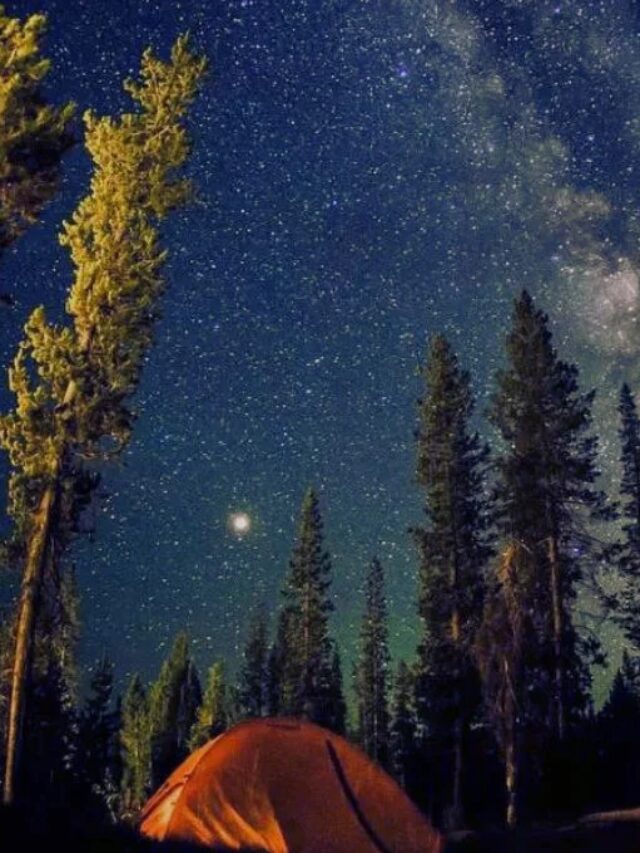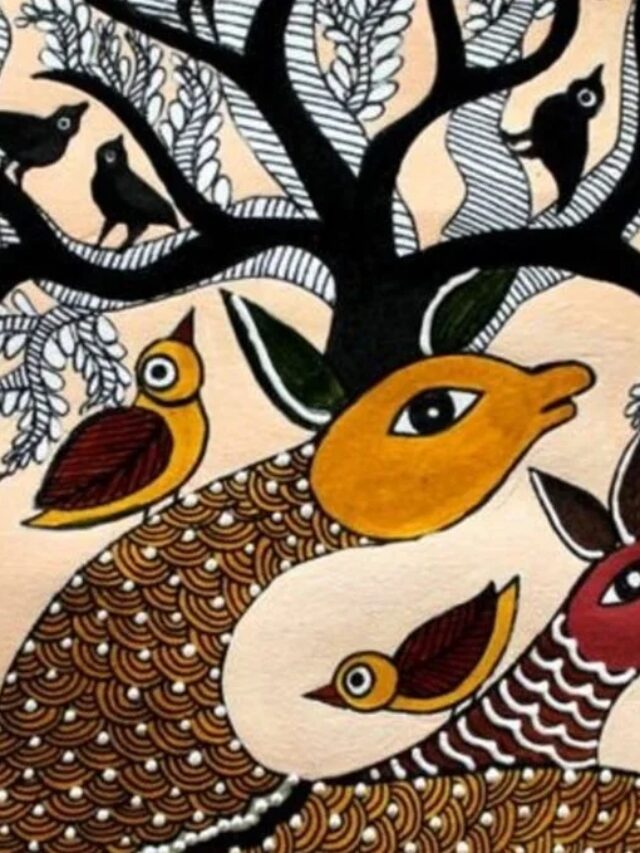क्या आप एक ऐसा घर चाहते हैं, जो आपके और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हो? मिट्टी के घर टिकाऊ, कम लागत वाले और सबसे खास बात यह है कि बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं।
क्या आप जानते हैं कि भारत में 118 मिलियन घरों में 65 मिलियन मिट्टी के घर हैं? हालांकि अधिकांश के पीछे आर्थिक कारण होते हैं लेकिन यह भी सच है कि बहुत से लोग मिट्टी के घरों को पसंद करते हैं क्योंकि इनसे कई फायदे मिलते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि धीरे-धीरे हमें शहरी क्षेत्रों में इस तरह के घर दिखने लगे हैं, घर के मालिकों को लगने लगा है कि उनके दादा-दादी के जमाने का घर ही बेहतर हैं। यहाँ तक कि लॉरी बेकर जैसे आर्किटेक्ट, जिन्हें ‘आर्किटेक्चर का गांधी‘ कहा जाता है, दशकों से इस चलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
(गांधी के विचारों को मानने वाले ब्रिटिश मूल के आर्किटेक्ट ने सैकड़ों मिट्टी के घरों का निर्माण किया और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए आर्किटेक्टों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया।)
आसानी से पहुंच और कम लागत होने के कारण सीमेंट और स्टील से अलग मिट्टी के घरों के कई फायदे हैं। आधुनिक सामग्रियों के विपरीत, वे दशकों बाद भी उसी अवस्था में खड़े रहते हैं और टूट जाने के बाद कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं।
इन 7 कारणों से मिट्टी की दीवारें मानी जाती हैं बेहतर
- मजबूत, कठोर और आपदा प्रतिरोधी

मिट्टी की ईंट एक बार स्थिर होने के बाद यह दीवारों और फर्श के लिए एक ठोस और टिकाऊ निर्माण सामग्री साबित हो सकती है। इसमें भूकंप या बाढ़ के दौरान भी दरारें नहीं आती हैं और सदियों तक टिका रह सकता है।
केरल के वास्तुकार यूजीन पंडला बताते हैं, “हालांकि मिट्टी के घरों में बारिश के दौरान कुछ समस्याएँ हो सकती हैं लेकिन निर्माण के दौरान ही इन समस्याओं को दुरुस्त किया जा सकता है। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए गेहूं की भूसी, पुआल, चूना और गाय के गोबर जैसे स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसे कि, स्टेब्लाइज्ड कंप्रेस्ड इंटरलॉकिंग अर्थब्लॉक (SCEB) तकनीक का उपयोग करके स्थानीय मिट्टी को पांच प्रतिशत सीमेंट के साथ स्टैबलाइज किया जा सकता है। इससे जो ईंट बनती है वह बहुत ही मजबूत और जल-प्रतिरोधक होती है।
इसका एक प्रमुख उदाहरण कच्छ में भुंगा है, जो भूकंप ग्रस्त क्षेत्र है। वहाँ घरों का निर्माण मिट्टी के ईंट, टहनियों और गोबर से गोलाकार संरचना में किया जाता है। इसी तरह, राजस्थान के बाड़मेर जिले में तीन तरह से घरों का निर्माण किया जाता है – बेलनाकार आकार, मिट्टी और छप्पर वाले छत।
इन घरों का निर्माण दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संगठन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) ने 2006 में विनाशकारी बाढ़ के बाद किया था। उस बाढ़ में हजारों घर उजड़ गए और सैकड़ों ग्रामीण बेघर हो गए थे।
- थर्मल इंसुलेशन

क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की दीवारों से बने घरों में किसी भी मौसम में अंदर सामान्य एवं आरामदायक तापमान कैसे होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी की दीवारें प्राकृतिक रूप से इंसुलेटेड होती हैं, जिससे घर के अंदर गर्मी से आराम मिलता है। गर्मियों के दौरान अंदर का तापमान कम होता है, जबकि सर्दियों में मिट्टी की दीवारें घर को गर्म रखती हैं और राहत देती हैं।
इसके अलावा छोटे-छोटे छिद्रों से भी ठंडी हवा घर में प्रवेश करती है। थाननल हैंड स्कल्प्टेड होम्स के सह-संस्थापक बीजू भास्कर कहते हैं, “मिट्टी के घर मानव शरीर के समान होते हैं। मिट्टी की दीवारें छिद्रपूर्ण होने के नाते, हमारी त्वचा की तरह सांस ले सकती हैं। यह अंदर के तापमान को आरामदायक बनाए रखने में मदद करता है, भले ही बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो। “
3.रीसाइकिल करने योग्य
जहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए रीसाइक्लिंग एक चर्चा का विषय बन गया है, वहीं मिट्टी के घर युगों से पर्यावरण के अनुकूल बने हुए हैं। ढहने के बाद भी मिट्टी के घर रिसाइकिल करने या पुन: उपयोग योग्य होते हैं। बीजू कहते हैं, “मिट्टी के घर की सामग्री को फिर से उपयोग किया जा सकता है और यदि आप इसे तोड़ते भी हैं तो यह फिर से मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए यदि आपका बेटा घर बनाना चाहता है तो वह पूरी सामग्री का फिर से इस्तेमाल कर सकता है और उसे कुछ नया मैटेरियल खोजने की जरूरत नहीं है। इस तरह, हम प्रकृति पर निर्माण के लिए निर्भरता को कम कर सकते हैं। ”
- बायोडिग्रेडेबल

तेजी से बढ़ते उपभोक्तावाद के कारण हम प्लास्टिक, धातु, कांच, और तांबे जैसी सामग्रियों से घिरे हुए हैं जिन्हें अपघटित होने में वर्षों लगते हैं। इसने हमारी धरती और जलाशयों पर टनों कचरे का बोझ बढ़ गया है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने से वे पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। मिट्टी सर्कुलर अर्थव्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आसानी से उसी प्रकृति में वापस चला जाता है, जहां से यह आया था।
- किफायती
मिट्टी या रैम्प्ड अर्थ को उचित दरों पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा यह स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री है जिससे परिवहन लागत की भी बचत होती है। पंडला कहते हैं , “अगर एक पारंपरिक घर बनाने में एक वर्ग फुट में 1,000 रुपये का खर्च आता है तो वहीं इको-फ्रेंडली घर में सिर्फ 600 रुपये ही खर्च होगा।“
- अनुकूलता

मिट्टी के घर बनाने के लिए चार बुनियादी निर्माण तकनीकें हैं जो जलवायु परिस्थितियों, स्थान और इसके आकार पर निर्भर करती हैं।
कॉब (Cob) : यह मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गाय के गोबर, घास, गोमूत्र और चूने का मिश्रण होता है जिसे औजारों, हाथों या पैरों से गूंथकर बनाया जाता है। इससे घर की नींव और दीवारें बनायी जाती हैं।
एडोब (Adobe): ईंटों को बनाने के लिए धूप में मिट्टी सुखायी जाती है।
टट्टर बांधना और पुताई (The Wattle and Daub) : लकड़ी / बांस की स्ट्रिप्स, जिसे टट्टर बाँधना कहा जाता है, इनकी मिट्टी, रेत, बजरी और चिकनी मिट्टी, आदि के घोल से पुताई की जाती है।
द रेम्ड अर्थ टेक्नीक (The rammed earth technique) : रेत, बजरी और मिट्टी के साथ-साथ कीचड़ के मिश्रण को तब तक रैम्प किया जाता है जब तक यह पत्थर की तरह ठोस न हो जाए।
मिट्टी को आसानी से अन्य सामग्रियों के साथ मिश्रित किया जा सकता है और इन सभी चार निर्माण तकनीकों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- कार्बन फुटप्रिंट

क्या आप जानते हैं कि सीमेंट उद्योग वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन का लगभग आठ प्रतिशत उत्पन्न करता है?
लंदन स्थित गैर-सरकारी संगठन चैथम हाउस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सीमेंट उद्योग को एक देश मान लिया जाए, तो यह 2.8 बिलियन टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश होता, इससे ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका ही होते।
21 वीं सदी में सीमेंट, मिट्टी का विकल्प बन गया और अधिकांश आर्किटेक्ट इसी का इस्तेमाल मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में करने लगे। इसकी तुलना में, मिट्टी में कार्बन फुटप्रिंट नगण्य हैं क्योंकि इसे रीसाइकिल किया जा सकता है और पृथ्वी से खुदाई करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह स्थानीय रूप से उपलब्ध है और परिवहन की जरूरत नहीं है (खदान से निर्माण स्थलों तक) जो बेवजह कार्बन उत्सर्जन बढ़ाते थे।
आप भी कम कार्बन उत्सर्जन वाला ऐसा घर चाहते हैं जो आपकी जेब पर भारी न पड़े, तो इस पर विचार कर सकते हैं।
मूल लेख-GOPI KARELIA
यह भी पढ़ें- स्वदेशी तकनीक और स्थानीय मज़दूर, ये आर्किटेक्ट कर चुके हैं बेहतर कल की शुरुआत
यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो हमें hindi@thebetterindia.com पर लिखें, या Facebook और Twitter पर संपर्क करें। आप हमें किसी भी प्रेरणात्मक ख़बर का वीडियो 7337854222 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: