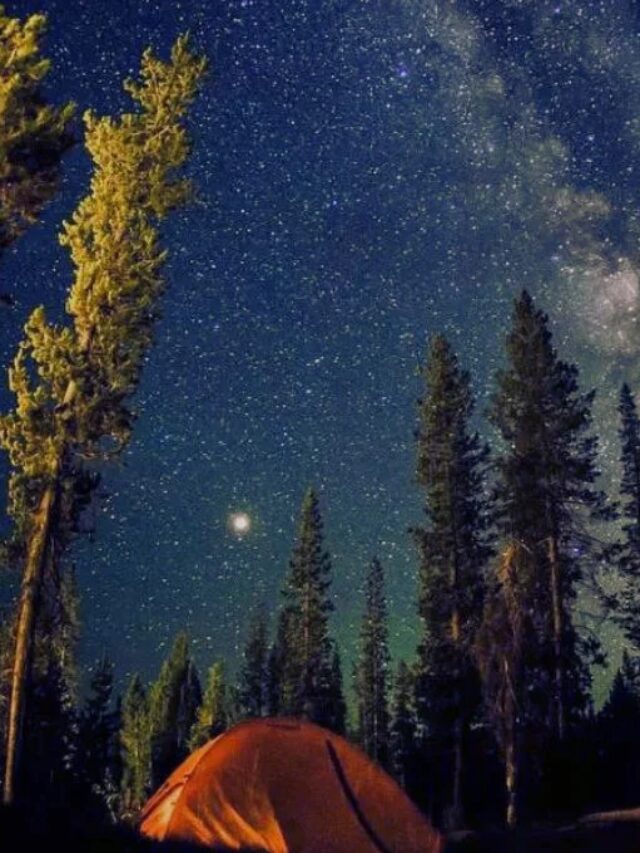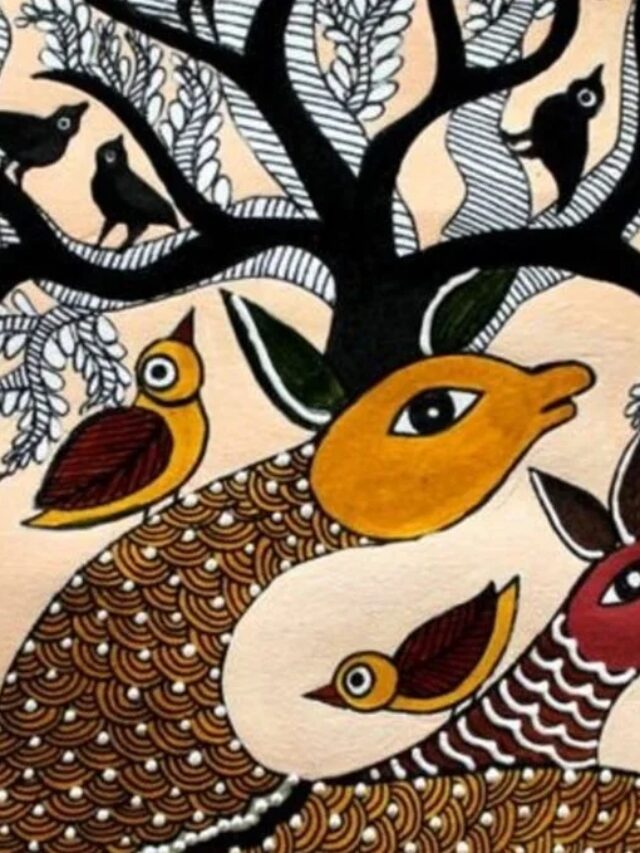जहां चाह, वहां राह! यह लाइन हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन चाह से राह तक के सफर को पूरा करने के लिए सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। काजीरंगा (असम) के छोटे से गाँव, बोसागांव में रहनेवाली रूपज्योति गोगोई (Roopjyoti Gogoi), प्लास्टिक को रीयूज़ करके बैग्स बनाती हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचानेवाले प्लास्टिक को कम करने के लिए, सीमित संसाधनों में उन्होंने अनोखा कदम उठाया।
वैसे तो रूपज्योति एक हाउस वाइफ हैं। लेकिन वह कई ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी हैं, जो कुछ नया और अलग करना तो चाहती हैं, लेकिन घर-परिवार की ज़िम्मेदारियां उनके कदमों को खींच लेती है। रूपज्योति ने प्लास्टिक बैग्स बनाने का फैसला कर, ना सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम उठाया। बल्कि अपने गाँव की कई महिलाओं को रोज़गार भी दिया।
कैसे हुई शुरुआत?
काज़ीरंगा नेशनल पार्क के पास रहनेवाली रूपज्योति ने, प्लास्टिक को दुबारा इस्तेमाल में लाने के लिए सुंदर व आसान तरीका खोजा। टूरिज्म के लिए मशहूर काज़ीरंगा के आस-पास काफ़ी सारा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है। प्रकृति की सुंदरता देखने आने वाले लोग, कई बार कहीं भी प्लास्टिक बॉटल या रैपर फेंककर इसे नुकसान पहुंचाते हैं।

रूपज्योति को लगा कि क्यों न इन प्लास्टिक्स से सुंदर चीज़ें बनाकर, इसे फिर से उपयोग में लिया जाए। इसके बाद उन्होंने काज़ीरंगा के अलग-अलग इलाकों से प्लास्टिक इकट्ठा करना शुरू किया और बुनाई करके सुंदर हैंडबैग, टेबल मैट, पांवदान, सजावट का सामान आदि बनाने लगीं।
कैसे और कब आया आइडिया?
रूपज्योति ने द बेटर इंडिया से बात करते हुए कहा, “मैं एक हाउस-वाइफ हूँ और हमारे गाँव में महिलाओं के लिए बहुत-सी पाबंदियां हैं। हमारे यहां औरतें ज्यादा पढ़ाई नहीं करतीं। गांव की सभी महिलाएं बहुत कम पढ़ी-लिखीं हैं। हम सारा दिन घर के कामों में ही लगे रहते हैं। अक्सर बाज़ार से जब सामान खरीदकर लाया जाता था, तो बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स और रैपर घर में इकट्ठा हो जाते थे। मुझे हमेशा लगता था कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए।”
उन्होंने आगे कहा, “जब एक बार दिमाग में कोई बात चलने लगती है, तो आपको हर जगह फिर वही नज़र आता है। मैं जब भी कभी बाहर निकलती थी, तो काज़ीरंगा नेशनल पार्क के आस-पास बहुत से पॉलिथीन दिखाई देते थे। मुझे लगता था कि घर और बाहर दोनों जगह इतनी सारी प्लास्टिक्स हैं, इन्हें कैसे कम किया जाए। अगर जलाते हैं, तो प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा और बाहर ऐसे ही फेंकने से वॉटर रिसोर्सेज़ और जानवरों को नुकसान पहुंचता है।”
इसके बाद, उन्होंने धीरे-धीरे इन पॉलिथीन्स को इकट्ठा करना शुरू किया। उनका कहना है कि गाँव की महिलाएं भले ही कम पढ़ी-लिखी हों, लेकिन उन्हें हैंडलूम का काम बहुत अच्छे से आता है। रूपज्योति ने उन सबसे बात की और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए तैयार किया।
2004 में शुरू की पहल

रूपज्योति ने द बेटर इंडिया को बताया, “वैसे तो मैं घर में प्लास्टिक से बैग, पांवदान वगैरह बनाती रहती थी। लेकिन साल 2004 में गाँव की महिलाओं के साथ हमने Village Waves के नाम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, इस काम को बड़े स्तर पर शुरू किया। क्योंकि उन्हें हैंडलूम का काम आता था, तो वे खुद जानती थीं कि क्या-क्या बनाया जा सकता है। मुझे मेरी माँ ने ही ये काम सिखाया था। वह मेरी बहुत मदद करती हैं।”
उन्होंने बताया, “गाँव की महिलाएं अपने घर पर ही ये काम करती हैं। इसलिए उनके घरवालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो मैं उन्हें प्लास्टिक से नई चीज़ें बनाने के साथ-साथ असम के ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल की बुनाई की ट्रेनिंग भी देती हूँ।”
कैसे तैयार होते हैं प्रोडक्ट्स?
सामान बनाने के लिये रूपज्योति हर तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं।

- रूपज्योति और अन्य महिलाएं सबसे पहले प्लास्टिक इकट्ठा कर, उन्हें अच्छे से साफ़ करती हैं।
- इसके बाद, प्लास्टिक को कैंची से काटकर आपस में जोड़-जोड़कर लंबा धागा जैसा बनाया जाता है।
- लूम के 2 हिस्से होते हैः ताना और बाना (warp weft)
- ताना पर धागा लगाया जाता है और बाना पर प्लास्टिक लगाते हैं। फिर इससे बुनाई कर, शीट्स तैयार करते हैं। फिर इन शीट्स से अलग-अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं।
बिजनेस नहीं, प्लास्टिक कम करना है मकसद
रूपज्योति का कहना है, “हम इस काम के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। सारे प्रोडक्ट की बुनाई लूम पर ही होती है। इसलिए बहुत देर तक हम काम नहीं करते। वैसे भी हमारा फोकस बिज़नेस नहीं है, हमें बस प्लास्टिक कम करना है। अगर बिजनेस और पैसों पर ध्यान देने लगे, तो प्लास्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी मांग बढ़ेगी। यही कारण है कि मैंने प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के अलावा असम के ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल की बुनाई का काम भी शुरू किया।”
साल 2004 में ही उन्होंने आर्टिस्टिक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर करवाया। जिसके तहत असम के पारंपरिक कपड़ों की बुनाई होती है। साथ ही, वह कपड़ों के बुनाई की ट्रेनिंग भी देती हैं। उनका कहना है, “हम यहां प्लास्टिक्स खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि हम भविष्य में ऐसा करने में सफल रहे, तो इससे जुड़े लोग बेरोज़गार नहीं होंगे। उनके पास कपड़ों की बुनाई का विकल्प है। वैसे भी असम के पारंपरिक हथकरघा और कपड़ा उत्पादों की अपने आप में जबरदस्त मांग है। लेकिन इसकी मांग और आपूर्ति के बीच हमेशा से एक बड़ा अंतर रहा है। ऐसे में, इससे महिलाओं को रोज़गार मिलता है और हम अपने पारंपरिक परिधानों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा भी पाते हैं।”
अब तक दे चुकीं है हज़ारों महिलाओं को ट्रेनिंग
रूपज्योति ने साल 2012 में काजीरंगा हाट की शुरुआत की थी। इस हाट में वह विलेज वेव्स के द्वारा बनाई गई चीज़ों को डिस्प्ले करती हैं। यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और अपने पसंद की चीज़ें खरीदकर ले भी जाते हैं। यह हाट रूपज्योति व उनके साथ काम करनेवाली महिलाओं की मेहनत का फल है। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए ही NEDFi (North Eastern Development Finance) ने उन्हें ये हाट दिया है। ताकि वे अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकें।
रूपज्योति अब तक असम और देशभर की 2300 से ज़्यादा महिलाओं को हैंडलूम और प्लास्टिक से अलग-अलग चीज़ें बनाने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। इनमें से कई महिलाओं ने तो अपना खुद का बिज़नेस भी शुरू कर लिया है।
सिर्फ 6 महीने ही होता है बिजनेस
रूपज्योति का कहना है, “यहां अक्टूबर/नवंबर से मई तक ही अच्छा बिजनेस होता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में टुरिस्ट कम ही आते हैं। इन 6 महीनों में हम 2 से 2.5 लाख का बिजनेस कर लेते हैं।”
वहीं उनके साथ काम करनेवाली दीपज्योति देका और कश्मीरी गोगोई ने बताया, “हमने जब से रूपज्योति के साथ काम करना शुरू किया है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हम नए लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। यहां आने वाले पर्यटकों से नई भाषाएं, नए कल्चर, नया अनुभव सीखने को मिलता है। साथ ही हमें यहां से जो पैसे मिलते हैं, उससे घर चलाने में मदद मिलती है। हमारा स्वाभिमान बढ़ता है, हमारे घर के पुरुष भी हमारी इज्जत करते हैं।”
गाँव में सड़क और बिजली की समस्या
रूपज्योति ने कहा, “गाँव में खराब सड़क होने के कारण बहुत परेशानी होती है। कभी-कभी तो इतना कीचड़ हो जाता है कि हमें कहीं आने-जाने में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा हमारे यहां बिजली भी बहुत कम समय के लिए ही आती है। हमारा काम हैंडलूम का है, जिसके लिए बिजली की ज़रूरत होती है।”

उन्होंने कहा कि गाँव की सारी औरतें जल्दी-जल्दी घर के सारे काम खत्म करके खाली हो जाती हैं। जब रात में या फिर सुबह उन्हें बिजली मिलती है, तो 3 से 4 घंटे वे बुनाई का काम करती हैं। रूपज्योति का कहना है, “मुझे नाम नहीं चाहिए और ना ही हमने सरकार से कभी कोई आर्थिक मदद मांगी है। लेकिन हम चाहते हैं कि गाँव को थोड़ी सुविधाएं मिलें। मेरी वजह से अगर गाँव का भला होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और हमें काम करने में भी आसानी हो जाएगी।”
वाकई रूपज्योति और उनके गाँव की महिलाएं बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। ऐसे में अगर वे किसी से थोड़े सपोर्ट की उम्मीद रखती हैं, तो इसके लिए आगे ज़रूर आना चाहिए। आप भी अगर कभी काज़ीरंगा जाएं, तो इस काज़ीरंगा हाट में ज़रूर जाएं और असम की कुछ ट्रेडिशनल व इको फ्रेंडली चीज़ें घर ले आएं।
अगर आप रूपज्योति व उनके टीम द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो Village Waves पर जा कर देख सकते हैं। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए 7896522593 पर कॉल भी कर सकते हैं।
संपादन- जी एन झा
ये भी पढ़ेंः किसान की तकनीक ने सहेजी GI Tagged Etikoppaka Toys बनाने की कला, बचाया 160 परिवारों का रोजगार
We at The Better India want to showcase everything that is working in this country. By using the power of constructive journalism, we want to change India – one story at a time. If you read us, like us and want this positive movement to grow, then do consider supporting us via the following buttons: